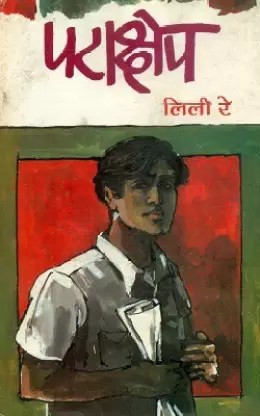
पुस्तक : पटाक्षेप, लेखिका लिली रे , साहित्यिकी प्रकाशन, संस्करण सन २०१५, ई. सं. २०७१, स्थान पटना, बिहार, कुल पृष्ठ १२८, आई. एस. बी. एन. 9789384394143, दाम १३० टाका
मैथिली भाषा में लिखित पटाक्षेप उपन्यास में लिली रे मुख्य रूप से 70 के दशक की नक्सलवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक और सामाजिक सन्दर्भ से परे पारिवारिक प्रभावों का मानवीय चित्रण पेश करती है। जहां एक तरफ विश्वविद्यालय परिसर में छात्र व्यवहार एवं बौद्धिक वर्ग जिनका विशेषकर झुकाव प्रगतिशील राजनीति से संबद्ध परिप्रेक्ष्य था और दूसरी ओर वह राजनीतिक परिदृश्य था जहां गैर बराबरी और गरिमा के प्रश्न आम समाज के सामने खड़े थे। समाज के उस दौर की इन चिंताओं में लिली रे अपने व्यक्तिगत अनुभव को बिहार सन्दर्भ में प्रस्तुत करती है चाहे उसमें उनके बेटे का नक्सलवादी आंदोलन में शरीक होने की घटना हो या उस जैसे कई घरों पर इस तरह के पड़ने वाले प्रभावों की परिकल्पना हो। यहाँ वह माँ भी है ,एक सूने घर-परिवार की सदस्या और उन भावों को अभिव्यक्त करती मुखर लेखिका भी। जिनका जीवन उस मुहाने पर आ खड़ा है जो राजनीतिक और सामाजिक सन्दर्भ में मानवीय पहलू को शामिल और उजागर करना अपना दायित्व समझती है।
लेखिका के उपन्यास की कहानी सार रूप से मुख्यतः तीन पात्रों अनिल, दिलीप और सुरजीत के इर्दगिर्द घूमती है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे, जिनमे एक किरदार स्वयं उनका पुत्र भी है। इन सभी की मित्रता कॉलेज में वैचारिक रूप से सामजिक एवं राजनितिक मुद्दों को लेकर बढ़ गई थी। उनका ये विश्वास प्रबल हो चूका था कि तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना से एक समता मूलक समाज की परिकल्पना कर पाना एक छलावा है और इसलिए समाज में आमूल चूल परिवर्तन लाने का एक मात्र रास्ता सशस्त्र विद्रोह है जिसकी झांकी नक्सलबाड़ी आंदोलन से निकलती है। युवा वर्ग में व्याप्त इन धारणाओं पर टिप्पणी करती हुई लेखिका उन बातों का भी जिक्र करती है कि कैंसे शहरी जीवन और ग्रामीण परिवेश की भिन्नता व ताना बाना एक अलग सामाजिकता है जिसे विशेष कर वो नौजवान, जिनका पारिवारिक और सामाजिक सम्बन्ध शहरों और समाज के ऊपरी वर्गों से है, नहीं समझ सकें। इस तरह वे लोग देहाती जीवन को जिस छायावादी समझ से देख पा रहे थे, ठीक उसके विपरीत जातिगत भेदभाव, आर्थिक गैरबराबरी और कुंठित सोच ग्रामीण जीवन का मुख्य हिस्सा थे। इस पृष्ठभूमि से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ सशस्त्र आन्दोलन क्यों सफल नहीं हुए और कैसे एक बेहतर कल की कल्पना अधूरी रही।
लेखिका बताती हैं कि पार्टी के उद्देश्यहित और इन सब मित्रों की एकमत राय थी कि हमारे इस लक्ष्य के लिए गाँव और देहात के लोगों को जागरूक और अपने साथ लाने के लिए उनको वहां के रहन सहन,भाषा और व्यवहार को समझना-अपनाना होगा। जिसके लिए ये बिहार के पूर्णिया जिले को केंद्र बनाते हैं जहां राजनीतिक और सामाजिक तौर पर कई समस्याएं हैं जैसे (1) व्यवहारिक और वैचारिक समस्या; जो मुख्यतः इनके खाने, रहने और भाषा के स्तर पर लोगों द्वारा इन्हें स्थानीय के तौर पर न देखना और पुलिस का भय (2) पार्टी के नेतृत्व में शहरी शिक्षित वर्ग के होने से स्थानीय लोगों का उनसे जुड़ने में असमर्थ होना (3) आमलोगों के ज़मीन से सांस्कृतिक सम्बन्ध और उसके साथ सामाजिक संबंधों को सही ढंग से नहीं समझे जाने का विरोधाभास (4) शहरी और ग्रामीण नेतृत्व व कैडर में उद्देश्य, व्यवहारिक अन्तराल तथा उनके व्यक्तिगत लाभ का स्पस्ट मतभेद व अन्तर (5) कुछ कैडरों का मुक्तिवाहिनी सेनाओं का साथ देना राज्य के साथ सहयोग करने जैसा था। जिससे कई बार यह फर्क़ दिखता था कि पुलिस का रवैय्या शहरी और ग्रामीण कैडर के लिए अलग अलग था जिससे एक विषम परिस्थितियां और दुविधा सामने दिखती है।
इन हालातों के मद्देनजर लेखिका स्पस्ट करती हैं कि इस सारी दिक्कतों और कुंठित, कलपित व नितांत कठोर जीवन ने इन तीनो मित्रों के भीतर भी एक संशय की स्थिति पैदा कर दी थी। इन्हे यह एक भूल लगने लगी थी कि यह आंदोलन जिसकी परिकल्पना उन्होंने जोर शोर से की थी वो जमीनी परिस्थितियों को समझे बगैर तैयार की गयी है।जैसे जब अलग अलग मौकों पर अनिल की मुलाकात दिलीप और सुजीत से होती है तो उनका एक दूसरे को यही जवाब होता था कि गलती शुरू से हुई है। इसी कारण से तीनो दोस्तों के संबंधों में भी एक खटास भर आई थी। इसलिए दिलीप जब आंदोलन छोड़ घर लौटता है तो उसे यह कडवा सच एक निर्वासन की भाँति प्रतीत होता है जिसे मुड कर देखना भी मुश्किल हो रहा है। इस तरह कैडर के बीच मानसिक स्वास्थ्य अब उत्पीड़न, खालीपन, चिंता और उद्देश्यहीनता जैसी बीमारी का शिकार हो रहा था।
इन सब के बीच लिली रे ने कुछ मानवीय मूल्यों को भी बखूबी सामने लाया है जैसे दिलीप को जब पहली बार चोरी की फसल लूटने का काम मिला तो उसे आपने पिता की याद आयी, जब उन्होंने किसी दोस्त की पेन्सिल ले आने पर उसकी पिटाई की थी और बासदेव की बीमार पत्नी के प्रति दिलीप का आवभगत। वैसे आंदोलन छोड़ने से पहले अनिल दिलीप को अपने साथ देखना चाहता है और उसके बगैर कुछ भी नहीं करना चाहता।
इस क्रम में जब लेखिका (माँ) को बेटे का खत मिलता है कि वह एम. ए. की फाइनल परीक्षा छोड़ नक्सलबादी आंदोलन में जा चूका है तो वह काफी दुखी और भयभीत हो जाती है। कुछ पारिवारिक मित्रों ने इसे बस एक फैशन कहा, जो कॉलेज के छात्रों में एक चलन की तरह था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जो इस आंदोलन में जाता है वह या तो मारा जाता है या फिर जेल जाता है। य़ह सब सुन लेखिका और भी टूट जाती है। वो अपने बेटे के निर्णय के सामने कुछ नहीं कर पाती। बस एक क्षोभ और उम्मीद के ख़त्म हो जाने का डर सही साबित होता नज़र आ रहा था। इस बीच एक बार जब दिलीप लौट कर घर आता भी है और चला जाता है तो लेखिका उसे जबर्दस्ती रोकने का प्रयास भी नहीं करती। क्योंकि दिलीप अपने दोस्त अनिल के बिना घर नहीं लौटना चाहता था।
लेखिका इस दौरान एक माँ और व्यक्ति के तौर पर खुद को अलग थलग पेश करती है। तथा कही भी बेटे पर खुद के विचार और निर्णय को थोपती नज़र नहीं आती।
लेखिका आंदोलन को छोड़ कर लौटने वाले सभी दोस्तों की कहानी भाव को एक माँ के तौर पर और इन पात्रों के माध्यम से बिलकुल ही सहज और सरलता से पेश करती है। लेखिका लिखती है कि उनके बेटे का लौटना उनके लिए एक दबी आवाज़ का फिर से उभारना जैसा था। लेकिन इतने दिनों के अंतराल पर लौटे बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं है और वो अब मानसिक रोग से ग्रसित है। माँ की चिंता उसके भविष्य को लेकर और भी बढ़ गई की क्या होगा जबकि पहले ही बेटे के नाम बड़ा करने की उम्मीदों पर पानी फिर चूका है। लेकिन उसके परे अब बेटे का स्वस्थ जीवन जीना भी दुस्वर था, ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक साथ कई स्वप्न का पटाक्षेप हो चूका है। बेहतर कल की कल्पना, बेटे से उम्मीद और बेटे की उम्मीद सब एक साथ ध्वस्त हो चुके थे।
बेटे और अपनी जिंदगी के पटाक्षेप का जवाब लिली रे आंदोलन के वैचारिक खोखलेपन में देखती है। लेखिका का मत तैयार होता है कि इस समाज में सशस्त्र बदलाव अपने आप में एक अकादमिक विषय था जिसे सक्रिय छात्रों ने काफी आगे बढ़ा दिया। उनके अंदर समाज की व्यावहारिक समझ की काफी कमी थीं। समाज के नीचे तबके के लोग राष्ट्र राज्य के हित में भी अपने हित साझा करते और व्यवस्था परिवर्तन एक धीमी और निरंतर कार्य है। लेकिन वामपंथी या नक्सलवादी आंदोलन आपने विचार और कार्यक्रमों में एकरूपता नहीं ला पाई, जिसका परिणाम आंदोलन का पटाक्षेप था। साथ ही साथ एक माँ के बेटे से लगी उम्मीद और नौजवानो का आंदोलन से मोह भंग और समतामूलक समाज की परिकल्पना का तत्काल अंत होना।
निष्कर्षत: मेरे ख्याल से 70 के दशक की झलक अभी हम विश्वविद्यालय और कुछ वामपंथी विचारधारों के लोगों के बीच देख सकते है। विचारधारा आज एक सामुहिक होड़ बन चुकी है जिसके पीछे कई समुदाय और संस्थाएँ नासमझ हो चल पड़ी है। क्योंकि विचारधारा की उपज अगर जागरूक समाज से हो तो इसका पीछे जनसमुदाय का दौड़ लगाना उचित है। क्या हमें नहीं लगता कि विचारधारा इतनी ज़रूरी न हो तो हम सबके प्रश्न और परिपेक्ष्य संवाद में शामिल कर पाएंगे। लेकिन विचारधारा का सामाजिक आधार से अलग कहीं राजनीतिक गलियारे में तैयार हो रहीं हो तो यह उस आम आदमी का निर्वासन कर देती है, जिनकी कोई परिपक्व समझ नहीं और और न ही की स्पस्ट विचारधारा।
लेकिन चीज़ें अब बदल गई है। शायद श्रमिक और खेतिहर मजदूरों के बीच के नाज़ुक फर्क को अब के बौद्धिक वर्ग ज्यादा बेहतर समझ पा रहें है। वर्तमान की वैश्विक आर्थिक नीतियों ने लोगों की उन बातों को ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से सामने लाया है जिसमें गावों की विवधता और जटिलता को समझना भी काफी महत्वपूर्ण है। बशर्ते यदि हम किसी बदलाव को लाना चाहते हो। साथ ही साथ ये भी काफी अहम् है कि ये माने की बदलाव एक कलेक्टिव कार्य है, इसमें व्यक्ति विशेष की नियत और सामाजिक परिदृश्य को समझे बिना आगे बढ़ना एक अंत की तरफ ही बढ़ना है।

शोधार्थी ,राजनीति अध्ययन केंद्र, जे.एन.यू.



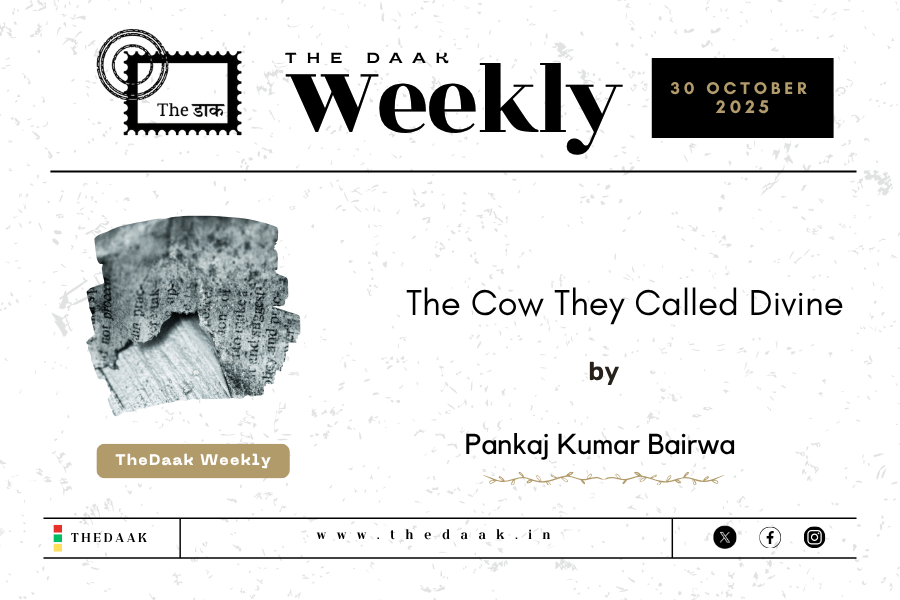
Leave a comment